पिछले
दो साल में हुए दो बड़े जनांदोलनों की छाया से सरकार बच नहीं पा रही है। यह छाया
21 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र पर भी पड़ेगी। इन आंदोलनों की नकारात्मक छाया
से बचने के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते दो बड़े फैसले किए हैं। केन्द्रीय कैबिनेट ने
पहले लोकपाल विधेयक के संशोधित प्रारूप को मंज़ूरी दी और उसके बाद स्त्रियों के खिलाफ
होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कानून में बदलाव की पहल करते हुए अध्यादेश लाने
का फैसला किया। दोनों मामलों में सरकार कुछ देर से चेती है और दोनों में उसका आधा-अधूरा
चिंतन दिखाई पड़ता है। अंदेशा यह है कि यह कदम उल्टा भी पड़ सकता है। सीपीएम ने इस
बात को सीधे-सीधे कह भी दिया है। यह अधूरापन केवल सरकार में नहीं समूची राजनीति में
है। इसके प्रमाण आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह
की याचिका पर छह साल पहले सरकार को निर्देश दिया था कि वह पुलिस सुधार का काम करे।
ज्यादातर राज्य सरकारों की दिलचस्पी इसमें नहीं है। पिछले साल लोकपाल आंदोलन को देखते
हुए लगभग सभी दलों ने संसद में आश्वसान दिया था कि कानून बनाया जाएगा। जब 2011 के दिसम्बर
में संसद में बहस की नौबत आई तो बिल लटक गया। सरकार अब जो विधेयक संशोधन के साथ लाने
वाली है उसके पास होने के बाद लोकपाल की परिकल्पना बदल चुकी होगी। दिसम्बर 2011 में
ही समयबद्ध सेवाएं पाने और शिकायतों की सुनवाई के नागरिकों के अधिकार का विधेयक भी
पेश किया गया था। कार्यस्थल पर यौन शोषण से स्त्रियों की रक्षा का विधेयक 2010 से अटका
पड़ा है। ह्विसिल ब्लोवर कानून के खिलाफ विधेयक अटका पड़ा है। भोजन का अधिकार विधेयक
अटका पड़ा है। यह संख्या बहुत बड़ी है।
Monday, February 4, 2013
Tuesday, January 29, 2013
विमर्श-विहीनता, विश्वरूपम से आशीष नन्दी तक

संयोग है कि आशीष नन्दी का प्रकरण तभी सामने आया, जब ‘विश्वरूपम’ पर चर्चा चल रही थी। आशीष नंदी
विसंगतियों को उभारते हैं। यह उनकी तर्क पद्धति है। वे मूलतः नहीं मानते कि पिछड़े
और दलित भ्रष्ट हैं, जैसा कि उनकी बात के एक अंश को सुनने से लगता है। वे मानते हैं
कि देश के प्रवर वर्ग का भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता। यह जयपुर लिटरेरी फोरम के मंच पर
कही गई गई थी। आशीष नन्दी से असहमति प्रकट करने के तमाम तरीके मौज़ूद हैं। पर सीधे
एफआईआर का मतलब क्या है? एक
मतलब यह कि विमर्श का नहीं कार्रवाई का विषय है। कार्रवाई होनी चाहिए। बेहतर हो कि
इस बहस को आगे बढ़ाएं, पर उसके पहले वह माहौल तो बनाएं जिसमें कोई व्यक्ति कुछ कहना
चाहे तो वह कह सके।
Monday, January 28, 2013
हेडली से ज्यादा हमें उसके सरपरस्तों की ज़रूरत है
अक्सर कुछ रहस्य कभी नहीं खुलते। कुछ में संकेत
मिल जाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। और कुछ में पूरी कहानी सामने होती, पर उसे
साबित किया नहीं जा सकता। 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमलों के साथ ऐसा
ही हुआ। पाकिस्तान के लश्करे तैयबा का इस मामले में हाथ होने और उसके कर्ता-धर्ताओं
के नाम सामने हैं। भारत में अजमल कसाब को स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर फाँसी दी जा चुकी
है। और अब अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को 35 साल
की सजा सुनाकर उन आरोपों की पुष्टि कर दी है। बावज़ूद इसके हम पाकिस्तान सरकार के सामने
साबित नहीं कर सकते हैं कि हमलों के सूत्रधार आपके देश में बाइज़्ज़त खुलेआम घूम रहे
हैं। अमेरिकी अदालत
में डेविड हेडली को सजा सुनाने वाले डिस्ट्रिक्ट जज ने अभियोजन पक्ष द्वारा हेडली के
लिए हल्की सजा की माँग किए जाने पर अपनी नाखुशी जाहिर की थी। सजा में पैरोल का कोई
प्रावधान नहीं है और दोषी को कम से कम 85 फीसदी सजा पूरी करनी होगी। 52 वर्षीय हेडली
जब जेल से बाहर आएगा तब उसकी उम्र 80 से 87 साल के बीच होगी। अमेरिकी अभियोजक उसके
लिए मौत या उम्र कैद की सजा भी माँग सकते थे, पर हेडली के साथ एक समझौते के तहत उन्होंने
यह सजा नहीं माँगी।
जज ने सजा सुनाते
हुए कहा हेडली आतंकवादी हैं। उसने अपराध को अंजाम दिया, अपराध में सहयोग किया और इस सहयोग के
लिए इनाम भी पाया। जज ने कहा, इस सजा से आतंकवादी रुकेंगे नहीं। वे इन सब बातों की
परवाह नहीं करते। मुझे हेडली की इस बात में कोई विश्वास नहीं होता जब वह यह कहता है
कि वह अब बदल गया। पर 35 साल की सजा सही सजा नहीं है। इसके पहले शिकागो की अदालत ने
इसी महीने की 18 तारीख को मुंबई हमले में शामिल हेडली के सहयोगी पाकिस्तानी मूल के
कनाडाई नागरिक 52 वर्षीय तहव्वुर राना को लश्कर-ए-तैयबा को साजो-सामान मुहैया कराने
और डेनमार्क के अखबार पर हमले के लिए षड्यंत्र में शामिल होने के लिए 14 साल की सजा
सुनाई गई थी। पर राना को मुम्बई मामले में शामिल होने के लिए सजा नहीं दी गई। इन दोनों
मामलों का दुखद पहलू यह है कि हमारे देश में हुए अपराध के लिए हम इन अपराधियों पर मुकदमा
नहीं चला सकते। हालांकि सरकार कह रही है कि हम हेडली और राना के प्रत्यर्पण की कोशिश
करेंगे, पर लगता नहीं कि प्रत्यर्पण होगा। अमेरिकी सरकार के अभियोजन विभाग ने हैडली
से सौदा किया था कि यदि वह महत्वपूर्ण जानकारियां देगा तो उसे भारत के हवाले नहीं किया
जाएगा। राना के मामले में अभियोजन पक्ष ने 30 साल की सजा माँगी थी, पर अदालत ने कहा,
सुनवाई के दौरान मिली जानकारियों और उपलब्ध कराई गई सामग्री को पढ़ने पर पता लगता है
कि राना एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जो लोगों
का मददगार भी है। यह समझना मुश्किल है कि इस तरह का व्यक्ति कैसे इतनी गहरी साजिश में
शामिल हो गया। दोनों मामलों में सजा देने वाले जज एक हैं शिकागो के डिस्ट्रिक्ट जज
हैरी डी लेनिनवेबर। हेडली और तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण में 1997 में अमरीका
से की गई संधि भी एक अड़चन है। यह संधि उस व्यक्ति की सुपुर्दगी की इजाजत नहीं देती
जो पहले ही उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका हो अथवा बरी हो चुका हो। प्रत्यर्पण संधि के तहत राना को इसलिए
सौंपा नहीं जा सकता, क्योंकि मुम्बई हमलों के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। हेडली इस दलील के साथ अपना
बचाव करेगा कि उसे दोषी ठहराया जा चुका है और वह सजा पा रहा है।
Saturday, January 26, 2013
राजनीति का चिंताहरण दौर
भारतीय राजनीति की डोर तमाम क्षेत्रीय, जातीय.
सामुदायिक, साम्प्रदायिक और व्यक्तिगत सामंती पहचानों के हाथ में है। और देश के दो
बड़े राष्ट्रीय दलों की डोर दो परिवारों के हाथों में है। एक है नेहरू-गांधी परिवार
और दूसरा संघ परिवार। ये दोनों परिवार इन्हें जोड़कर रखते हैं और राजनेता इनसे जुड़कर
रहने में ही समझदारी समझते हैं। मौका लगने पर दोनों ही एक-दूसरे को उसके परिवार की
नसीहतें देते हैं। जैसे राहुल गांधी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने पर भाजपा ने वंशवाद
को निशाना बनाया और जवाब में कांग्रेस ने संघ की लानत-मलामत कर दी। जयपुर चिंतन शिविर
में उपाध्यक्ष का औपचारिक पद हासिल करने के बाद राहुल गांधी ने भावुक हृदय से मर्मस्पर्शी
भाषण दिया। इसके पहले सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि समय की
ज़रूरतों को देखते हुए वे आत्ममंथन करें। नगाड़ों और पटाखों के साथ राहुल का स्वागत
हो रहा था। पर उसके पहले गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे के एक वक्तव्य ने विमर्श की
दिशा बदल दी। इस हफ्ते बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव भी तय था। चुनाव के ठीक पहले गडकरी
जी से जुड़ी कम्पनियों में आयकर की तफतीश शुरू हो गई। इसकी पटकथा भी किसी ने कहीं लिखी
थी। इन दोनों घटनाओं का असर एक साथ पड़ा। गडकरी जी की अध्यक्षता चली गई। राजनाथ सिंह
पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में उभर कर आए हैं। पर न तो राहुल के पदारोहण का जश्न
मुकम्मल हुआ और न गडकरी के पराभव से भाजपा को कोई बड़ा धक्का लगा।
Friday, January 25, 2013
कोई बताए हमारा आर्थिक मॉडल क्या हो
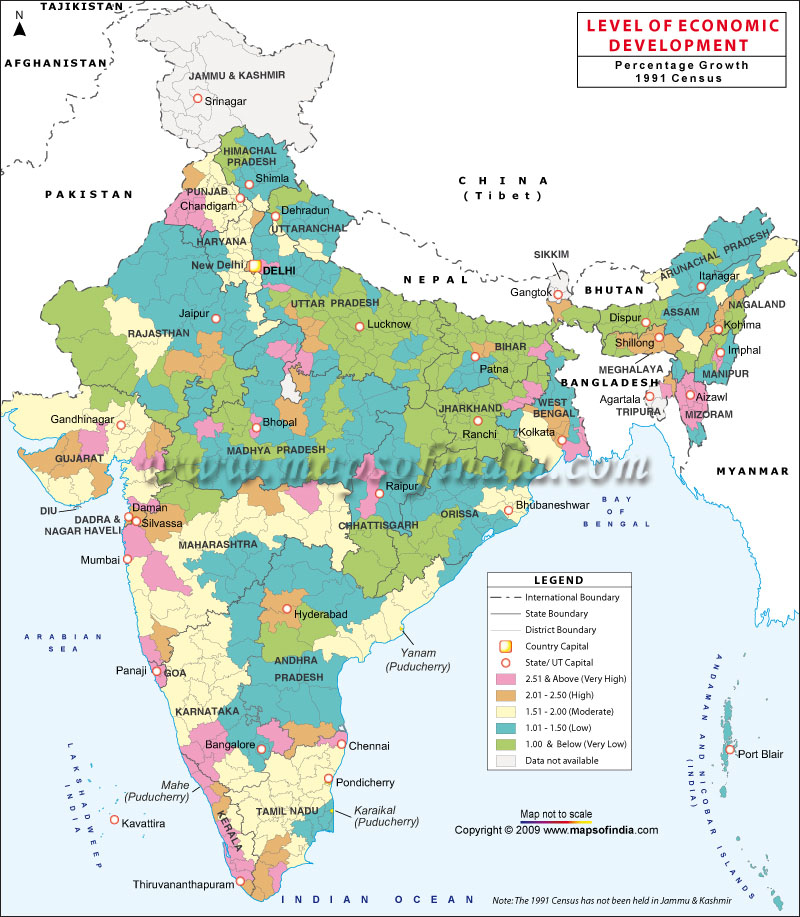
समकालीन सरोकार, जनवरी 2013 में प्रकाशित
सन 2013 का पहला सवाल है कि क्या इस साल लोकसभा चुनाव होंगे? लोकसभा चुनाव नहीं भी हों, आठ विधान सभाओं के चुनाव होंगे। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक का अलग-अलग कारणों से राजनीतिक महत्व है। सवाल है क्या दिल्ली की गद्दी पर गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा सरकार आने की कोई सम्भावना बन रही है? संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने एफडीआई के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता हासिल की है। इसके अलावा बैंकिग विधेयक लोकसभा से पास भी करा लिया है। अभी इंश्योरेंस, पेंशन और भूमि अधिग्रहण कानूनों को पास कराना बाकी है। और जैसा कि नज़र आता है कांग्रेस और भाजपा आर्थिक उदारीकरण के एजेंडा को मिलकर पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात विचित्र लगेगी कि एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी ताकतें किस तरह एक-दूसरे का सहयोग कर रही है, पर बैंकिंग विधेयक में दोनों का सहयोग साफ दिखाई पड़ा। खुदरा बाज़ार में एफडीआई को लेकर सरकार पहले तो नियम 184 के तहत बहस कराने को तैयार नहीं थी, पर जैसे ही उसे यह समझ में आया कि सरकार गिराने की इच्छा किसी दल में नहीं है, वह न सिर्फ बहस को तैयार हुई, बल्कि उसपर मतदान कराया और जीत हासिल की। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी इसे मैन्युफैक्चरिंग मेजॉरिटी कहते हैं, पर संसदीय लोकतंत्र यही है। सन 1991 में आई पीवी नरसिंह राव की सरकार कई मानों में विलक्षण थी। हालांकि आज़ादी के बाद से हर दशक ने किसी न किसी किस्म के तूफानों को देखा है, पर नरसिंह राव की सरकार के सामने जो चुनौतियाँ थी वे आसान नहीं थीं। उनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, जिसके बाद देश भर में साम्प्रदायिक हिंसा का जबर्दस्त दौर चला। मुम्बई में आतंकी धमाकों का चक्र उन्ही दिनों शुरू हुआ। कश्मीर में सीमापार से आतंकवादी कार्रवाइयों का सबसे ताकतवर सिलसिला तभी शुरू हुआ। पर हम नरसिंह राव सरकार को उन आर्थिक उदारवादी नीतियों के कारण याद रखते हैं, जिनका प्रभाव आज तक है। भारत में वैश्वीकरण की गाड़ी तभी से चलनी शुरू हुई है। वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस सरकार के वित्त मंत्री थे। जब पहली बार आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया गया था तब कई तरह की आशंकाएं थीं। मराकेश समझौते के बाद जब 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना तब भी इन आशंकाओं को दोहराया गया। पिछले इक्कीस साल में इन अंदेशों को बार-बार मुखर होने का मौका मिला, पर आर्थिक उदारीकरण का रास्ता बंद नहीं हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के बाद संयुक्त मोर्चा और एनडीए की सरकारें बनीं। वे भी उसी रास्ते पर चलीं। बंगाल और केरल में वाम मोर्चे की सरकारें आईं और गईं। उन्होंने भी उदारीकरण की राह ही पकड़ी। मुख्यधारा की राजनीति में उदारीकरण की बड़ी रोचक तस्वीर बनी है। ज्यादातर बड़े नेता उदारीकरण का खुला समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि विरोध करते हैं। पर सत्ता में आते ही उनकी नीतियाँ वैश्वीकरण के अनुरूप हो जाती हैं। एफडीआई पर संसद में हुई बहस की रिकॉर्डिंग फिर से सुनें तो आपको परिणाम को लेकर आश्चर्य होगा, पर राजनीति इसी का नाम है। उदारीकरण के दो दशकों का अनुभव यह है कि हम न तो उसके मुखर समर्थक हैं और न व्यावहारिक विरोधी। इस अधूरेपन का फायदा या नुकसान भी अधूरा है।
Subscribe to:
Comments (Atom)



