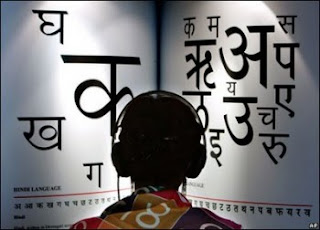इस हफ्ते भारतीय मीडिया पर जिम्मेदारी का दबाव है। 24 सितम्बर को बाबरी मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। उसके बाद कॉमनवैल्थ गेम्स शुरू होने वाले हैं, जिन्हें लेकर मस्ती कम अंदेशा ज्यादा है। पुरानी दिल्ली में इंडियन मुज़ाहिदीन ने गोली चलाकर इस अंदेशे को बढ़ा दिया है। कश्मीर में माहौल बिगड़ रहा है। नक्सली हिंसा बढ़ रही है और अब सामने हैं बिहार के चुनाव। भारत में मीडिया, सरकार और समाज का द्वंद हमेशा रहा है। इतने बड़े देश के अंतर्विरोधों की सूची लम्बी है। मीडिया सरकार को कोसता है, सरकार मीडिया को। और दर्शक या पाठक दोनों को।
न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अयोध्या मसले को लेकर पहले से सावधानी बरतने का फैसला किया है। फैसले की खबर देते समय साथ में अपनी राय देने या उसका निहितार्थ निकालने की कोशिश नहीं की जाएगी। बाबरी विध्वंस की फुटेज नहीं दिखाई जाएगी। इसके अलावा फैसला आने पर उसके स्वागत या विरोध से जुड़े विज़ुअल नहीं दिखाए जाएंगे। यानी टोन डाउन करेंगे। हाल में अमेरिका में किसी ने पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को जलाने की धमकी दी थी। उस मामले को भी हमारे मीडिया ने बहुत महत्व नहीं दिया। टकराव के हालात में मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मीडिया ने इसे समझा यह अच्छी बात है।
6 दिसम्बर 1992 को देश में टीवी का प्रसार इस तरीके का नहीं था। प्राइवेट चैनल के नाम पर बीबीसी का मामूली सा प्रसारण केबल टीवी पर होता था। स्टार और एमटीवी जैसे चैनल थे। सब अंग्रेजी में। इनके बीच ज़ी का हिन्दी मनोरंजन चैनल प्रकट हुआ। अयोध्या ध्वंस के काफी बाद भारतीय न्यूज़ चैनल सामने आए। पर हम 1991 के इराक युद्ध की सीएनएन कवरेज से परिचित थे, और उससे रूबरू होने को व्यग्र थे। उन दिनों लोग न्यूज़ ट्रैक के कैसेट किराए पर लेकर देखते थे। आरक्षण-विरोधी आंदोलन के दौरान आत्मदाह के एक प्रयास के विजुअल पूरे समाज पर किस तरह का असर डालते हैं, यह हमने तभी देखा। हरियाणा के महम में हुई हिंसा के विजुअल्स ने दर्शकों को विचलित किया। अखबारों में पढ़ने के मुकाबले उसे देखना कहीं ज्यादा असरदार था। पर ज्यादातर मामलों में यह असर नकारात्मक साबित हुआ।
बहरहाल दिसम्बर 1992 में मीडिया माने अखबार होते थे। और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण थे हिन्दी के अखबार। 1992 के एक साल पहले नवम्बर 1991 में बाबरी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश हुई थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, ऐसी घटना नहीं हुई। मुझे याद है लखनऊ के नव भारत टाइम्स ने बाबरी के शिखर की वह तस्वीर हाफ पेज में छापी। सबेरे उस अखबार की कॉपियाँ ढूँढे नहीं मिल रहीं थीं। उस ज़माने तक बहुत सी बातें मीडिया की निगाहों से दूर थीं। आज मीडिया की दृष्टि तेज़ है। पहले से बेहतर तकनीक उपलब्ध है। तब के अखबारों के फोटोग्राफरों के कैमरों के टेली लेंसों के मुकाबले आज के मामूली कैमरों के लेंस बेहतर हैं।
मीडिया के विकास के समानांतर सामाजिक-अंतर्विरोधों के खुलने की प्रक्रिया भी चल रही है। साठ के दशक तक मुल्क अपेक्षाकृत आराम से चल रहा था। सत्तर के दशक में तीन बड़े आंदोलनों की बुनियाद पड़ी। एक, नक्सली आंदोलन, दूसरा बिहार और गुजरात में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और तीसरा पंजाब में अकाली आंदोलन। तीनों आंदोलनों के भटकाव भी फौरन सामने आए। संयोग है कि भारतीय भाषाओं के, खासकर हिन्दी के अखबारों का उदय इसी दौरान हुआ। यह जनांदोलनों का दौर था। इसी दौरान इमर्जेंसी लगी और अखबारों को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। इमर्जेंसी हटने के बाद देश के सामाजिक-सांस्कृतिक अंतर्विरोधों ने और तेजी के साथ एक के बाद एक खुलना शुरू किया। यह क्रम अभी जारी है।
राष्ट्रीय कंट्राडिक्शंस के तीखे होने और खुलने के समानांतर मीडिया के कारोबार का विस्तार भी हुआ। मीडिया-विस्तार का यह पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके कारण मीडिया को अपनी भूमिका को लेकर बातचीत करने का मौका नहीं मिला। बाबरी-विध्वंस के बाद देशभर में विचार-विमर्श की लहर चली थी। अखबारों की भूमिका की खुलकर और नाम लेकर निंदा हुई। उस तरीके का सामाजिक संवाद उसके बाद नहीं हुआ। अलबत्ता उस संवाद का फायदा यह हुआ कि आज मीडिया अपनी मर्यादा रेखाएं तय कर रहा है।
सामाजिक जिम्मेदारियों को किनारे रखकर मीडिया का विस्तार सम्भव नहीं है। मीडिया विचार-विमर्श का वाहक है, विचार-निर्धारक या निर्देशक नहीं। अंततः विचार समाज का है। यदि हम समाज के विचार को सामने लाने में मददगार होंगे तो वह भूमिका सकारात्मक होगी। विचार नहीं आने देंगे तो वह भूमिका नकारात्मक होगी और हमारी साख को कम करेगी। हमारे प्रसार-क्षेत्र के विस्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण है साख का विस्तार। तेज बोलने, चीखने, कूदने और नाचने से साख नहीं बनती। धीमे बोलने से भी बन सकती है। शॉर्ट कट खोजने के बजाय साख बढ़ाने की कोशिश लम्बा रास्ता साबित होगी, पर कारोबार को बढ़ाने की बेहतर राह वही है।
खबर के साथ बेमतलब अपने विचार न देना, उसे तोड़ कर पेश न करना, सनसनी फैलाने वाले वक्तव्यों को तवज्जो न देना पत्रकारिता के सामान्य सूत्र हैं। पिछले बीस बरस में भारतीय मीडिया जातीय, साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय मसलों से जूझ रहा है। इससे जो आम राय बनकर निकली है वह इस मीडिया को शत प्रतिशत साखदार भले न बनाती हो, पर वह उसे कूड़े में भी नहीं डालती। जॉर्ज बुश ने कहीं इस बात का जिक्र किया था कि अल-कायदा के नेटवर्क में भारतीय मुसलमान नहीं हैं। इसे मीडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें। भारतीय मुसलमान के सामने तमाम दुश्वारियाँ हैं। वह आर्थिक दिक्कतों के अलावा केवल मुसलमान होने की सज़ा भी भुगतता है, पर भारतीय राष्ट्र राज्य पर उसकी आस्था है। इस आस्था को कायम रखने में मीडिया की भी भूमिका है, गोकि यह भूमिका और बेहतर हो सकती है। कश्मीर के मामले में भारतीय मुसलमान हमारे साथ है।
मीडिया सामजिक दर्पण है। जैसा समाज सोचेगा वैसा उसका मीडिया होगा। यह दोतरफा रिश्ता है। मीडिया भी समाज को समझदार या गैर-समझदार बनाता है। हमारी दिलचस्पी इस बात में होनी चाहिए कि हम किस तरह सकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं। साथ ही इस बात में कि हमारे किसी काम का उल्टा असर न हो। उम्मीद है आने वाला वक्त बेहतर समझदारी का होगा। पूरा देश हमें देखता, सुनता और पढ़ता है।