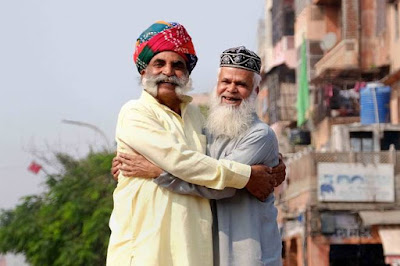भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार
सिंह भदौरिया ने इस साल के वायुसेना दिवस के ठीक पहले कहा कि भारत की योजना अब
विदेशी लड़ाकू विमानों के आयात की नहीं है और हम अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए या
एम्का) के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनका यह वक्तव्य अनेक कारणों से
महत्वपूर्ण है और इससे देश की रक्षा प्राथमिकताओं पर प्रकाश भी पड़ता है, पर उससे
पहले सवाल है कि स्वतंत्रता के 72 साल बाद आज हम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? हमने पहले ही स्वदेशी तकनीक के विकास पर ध्यान क्यों नहीं दिया?
सवाल यह भी है कि क्या पाँचवीं पीढ़ी के विमान का विकास
करने की तकनीकी सामर्थ्य हमारे पास है? प्रश्न केवल
स्वदेशी युद्धक विमान का ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर
होने का है। रक्षा के क्षेत्र में बेहद जटिल और उच्चस्तरीय तकनीकों और उसमें
समन्वय और सहयोग की जरूरत भी होती है। दुनिया में कोई भी संस्था ऐसी नहीं है, जो
पूरा लड़ाकू विमान तैयार करती हो। विमान के अलग-अलग अंगों को कई तरह की संस्थाएं
विकसित करती हैं। विमान की परिकल्पना और विभिन्न उपकरणों को जोड़कर विमान बनाना
(इंटीग्रेशन) और उपकरणों की आपूर्ति का इंतजाम करने की महारत भी आपके पास होनी
चाहिए।
निजी क्षेत्र की भागीदारी
रक्षा तकनीक खुले बाजार में नहीं बिकती। उसके लिए सरकारों
के साथ समन्वय करना होता है। दुनियाभर में सरकारें रक्षा-तकनीक को नियंत्रित करती
हैं। यह सच है कि हम अपनी रक्षा आवश्यकताओं की 60-65 फीसदी आपूर्ति विदेशी सामग्री
से करते हैं। दूसरी तरफ यह भी सच है कि विकासशील देशों में भारत ही ऐसा देश है,
जिसके पास रक्षा उत्पादन का विशाल आधार-तंत्र है। हमारे पास रक्षा अनुसंधान विकास से जुड़े
संस्थान हैं, जिनमें सबसे बड़ा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) संगठन है।